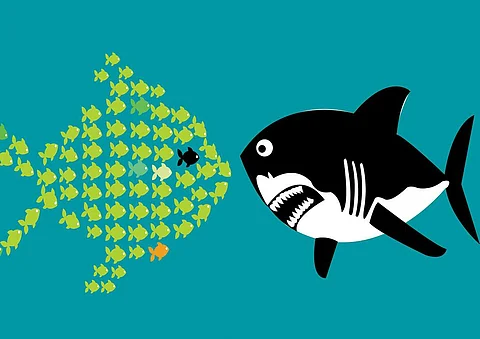
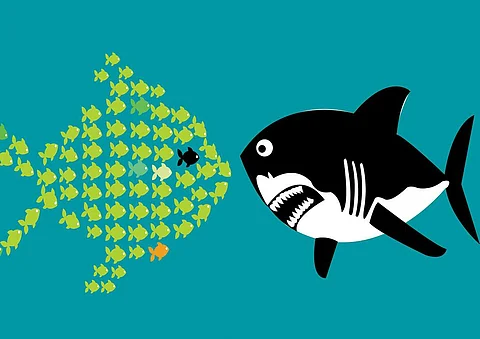
आम चुनाव की घोषणा होने के साथ ही सिविल सोसायटी समूह राजनीति के हिसाब-किताब में जुट गए हैं। राजनीतिक दल और ये समूह दोनों की एक-दूसरे से आस लगाए हुए हैं। जहां एक ओर राजनीतिक दल ऐसे समुदायों के साथ सुनियोजित बातचीत एवं चर्चा शुरू कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ये समूह अपने हितों को राजनीतिक दलों के घोषणा-पत्र और चुनाव अभियान में शामिल करने की जुगत लगा रहे हैं।
मार्च में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एनजीओ, वन समुदायों से संबंधित कार्य समूहों, पर्यावरणविदों और अन्य जन अभियानों से जुड़े लोगों के साथ दिल्ली और गोवा में कई बैठकें कीं। इससे पहले पिछले वर्ष दिसंबर में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में राज्य विधानसभा चुनावों से पहले ऐसे समूहों तक पहुंचने के लिए एक इकाई का गठन किया था। यद्यपि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को इन समूहों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए नहीं जाना जाता, तथापि इस दल ने भी अपने प्रमुख सदस्यों को ऐसे समूहों, विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े समूहों तक पहुंच बनाने के लिए छोटे कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया है। ये समूह हमेशा से कम्युनिस्ट पार्टी के अभियान और बहस का हिस्सा रहे हैं।
हाल के वर्षों में, खासकर वर्ष 2012-14 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में चलाए गए भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के जन्म तथा 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में इस पार्टी ने शानदार जीत ने सिविल सोसायटी समूहों के राजनीतिक और चुनावी महत्व को चर्चा का विषय बना दिया। इस चर्चा के दो मुद्दे हैं। पहला, क्या ऐसे समूहों को राजनीति में आना चाहिए और दूसरा मुद्दा यह कि क्या ऐसे समूहों और राजनीतिक दलों के बीच संपर्क आवश्यक है।
आमतौर पर हम संस्कृति, पर्यावरण और शिक्षा से जुड़े कार्यकर्ताओं को सिविल सोसायटी का हिस्सा मानते हैं। उन्हें ये नाम देना तर्कसंगत भी है। लेकिन ये सामाजिक सक्रियता की राजनीतिक प्रकृति का मुखौटा भी हैं। यह लोगों में यह भ्रम पैदा करता है कि सामाजिक कार्यकर्ता राजनीतिक व्यक्ति नहीं होते। सामाजिक सक्रियता या तो सरकार के विरुद्ध होती है या फिर सरकार से इसका कोई न कोई संबंध होता है। राजनीतिक और सामाजिक सक्रियता के बीच जो विभाजन रेखा है वह झूठी है। लेकिन मंझे हुए राजनेता किसी भ्रम में नहीं रहते। उन्हें इन सामाजिक कार्यकर्ताओं से लगातार निपटना पड़ता है जो जनता की नब्ज को पहचानने का दावा करते हैं। राजनेता इस बात से हमेशा चिढ़ते हैं और चुनाव के हथियार से सामाजिक कार्यकर्ताओं के समक्ष चुनौती पैदा करते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले अरविंद केजरीवाल ने सिविल सोसायटी के चुनावी राजनीति के साथ प्रयोग के अहम दौर के चरमोत्कर्ष को दर्शाया है। कुछ हद तक केजरीवाल सिविल सोयायटी और चुनावी राजनीति की अल्प ज्ञात लेकिन पुराने समय से चली आ रही गुप्त सांठ-गांठ का नवीनतम रूप हैं। और इसका कारण है देश में चुनावी लोकतंत्र का गिरता स्तर।
धनबल और बाहुबल का वर्चस्व
एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के संस्थापक अध्यक्ष और भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलोर में परिमापक पद्धति और सूचना प्रणाली के प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री द्वारा किए गए अध्ययन “सिविल सोसायटी, इंडियन इलेक्शंस एंड डेमोक्रेसी टुडे” के अनुसार, चुनाव में जीत का फैसला धनबल और बाहुबल से होता है। इस अध्ययन में वर्ष 2004 से 2014 तक उम्मीदवारों और विजेताओं के 60,000 रिकॉर्डों का विश्लेषण किया गया है जिसके अनुसार साफ छवि वाले केवल 12 प्रतिशत उम्मीदवार जीते थे जबकि जीतने वाले लगभग 23 प्रतिशत उम्मीदवार दागदार छवि वाले तथा 23 प्रतिशत विजेताओं पर तो गंभीर आरोप थे। उम्मीदवारों की औसत संपत्ति (2004-2014) 1.37 करोड़ रुपए थी, तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवारों की संपत्ति 2.03 करोड़ रुपए, दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवारों की संपत्ति 2.47 रुपए करोड़ रुपए और जीतने वाले उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 3.8 करोड़ रुपए थी।
इससे साफ पता चलता है कि ज्यादा पैसे वाले उम्मीदवारों को ज्यादा वोट मिले हैं और चुनावों में ज्यादा जीत भी मिली है। इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, लेकिन पिछले 10 वर्षों के दौरान 62,800 से अधिक उम्मीदवारों के व्यापक रुझान बिल्कुल स्पष्ट हैं। अपराध और पैसे का गठजोड़ ज्यादा खतरनाक साबित हुआ है। आपराधिक रिकॉर्ड वाले विजेताओं की औसत संपत्ति 4.27 करोड़ रुपए थी जबकि गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड वाले विजेताओं की औसत संपत्ति 4.38 करोड़ रुपए थी।
आंदोलन का रास्ता
सिविल सोसायटी समूह उपरोक्त रुझानों के आधार पर चुनाव लड़ने के लिए सही उम्मीदवार और सही एजेंडे की मांग करते रहे हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर कहती हैं, “चुनाव ऐसा मुद्दा है जिसके लिए कोई भी कार्यकर्ता खड़ा हो सकता है। किसी उम्मीदवार की जीत या हार को ही हालिया चुनावों में उसकी भागीदारी का मापदंड नहीं बनाना चाहिए। अंतत: ऐसी भागीदारी चुनावों में पैसे के इस्तेमाल पर गंभीर सवाल खड़े कर सकती है और चुनाव सुधार का कारण बन सकती है।” वर्तमान में यह पता लगाने के लिए कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि ऐसे कितने उम्मीदवार या समूह चुनाव में हिस्सा लेंगे। लेकिन 2014 में भारत में सबसे ज्यादा पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा था। इसका श्रेय आम आदमी पार्टी को जाता है जिसने 400 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े किए थे। इनमें से लगभग 110 उम्मीदवार पर्यावरणीय मुद्दों पर कार्य कर रहे थे। हालांकि इनमें से अधिकांश जीत नहीं पाए, तथापि संसदीय चुनावों में भी स्थानीय मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी।
पहले भी सामाजिक आंदोलन के कई नेताओं ने जनता के सशक्तिकरण के व्यापक लक्ष्य को हासिल करने के लिए चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। लेकिन सर्वसम्मति के कारण उनकी इच्छा पूरी न हो सकी और चुनावों से दूर रहना सिविल सोसायटी के आंदोलनों की मुख्य रणनीति बनी रही।
भारत में कई ऐसे जन आंदोलन हुए जिसने राजनीतिक पहचान ले ली, बल्कि इनमें से अधिकांश ने इसे अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे प्रयोगों का लंबा इतिहास रहा है। इनमें से अधिकांश प्रयोग स्थानीय संसाधनों पर अधिकार से जुड़े थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रयोग शासन और राजनीतिक के अंतर से अछूते थे। अन्य चीजों के अलावा ये आंदोलन भूमि, वन और पानी पर जनता का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राजनीति परिवर्तन की मांग करते हैं। ये चुनावी कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं जिनमें राजनेताओं के बीच अपने एजेंडा का प्रचार करना शामिल है। इनकी चुनावी सफलता नगण्य है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के प्रयोग शुरुआत के रूप में देखे जाते रहेंगे।
1970 के दशक की शुरुआत में जयप्रकाश नारायण (जेपी) द्वारा चलाए गए पूर्ण क्रांति आंदोलन ने 1975-77 के आपातकाल को जन्म दिया। आपातकाल के बाद जब 1978 में दिल्ली में जनता पार्टी सरकार का प्रयोग विफल होने लगा, तो जेपी आंदोलन के कई कार्यकर्ताओं ने समाज सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पूरी करने के तरीके ढूंढने शुरू कर दिए। इसी से संगठन बनाकर स्वैच्छिक कार्रवाई करने का दौर शुरू हुआ। सिविल सोसायटी का वर्तमान नाम (अथवा इसका चिंताजनक विकल्प ‘गैर-सरकारी कर्ता’) 1990 के दशक से इस्तेमाल में आना शुरू हुआ।
जब कांग्रेस सत्ता में लौटी तो तत्कालीन प्रधानमंत्री (इंदिरा गांधी) ने आपातकाल के दौरान और उसके बाद गांधीवादी स्वैच्छिक एजेंसियों और जनता पार्टी के नेताओं के बीच सांठगांठ की जांच के लिए कुदाल आयोग का गठन किया था। अगले छ: महीनों के दौरान कुदाल आयोग द्वारा किए गए उत्पीडन ने ऐसे संगठनों और कार्यकर्ताओं के बेहतरीन कार्य को “बर्बाद” कर दिया।
तब से स्वैच्छिक संगठनों के अनेक नेताओं ने कई बार औपचारिक चुनावी राजनीति में भाग लेने की कोशिश की। 1990 के दशक की शुरुआत में आंध्र प्रदेश में अवेयर (एक्शन फॉर वेलफेयर एंड अवेकनिंग इन रूरल एनवायरमेंट) और कुछ अन्य व्यक्तियों के उदाहरण यह दर्शाते हैं कि भारत की जनता आमतौर पर सिविल सोसायटी के नेताओं की चुनावी महत्वाकांक्षा का समर्थन नहीं करती है, विशेष रूप से तब, जब वे विधानसभा या संसदीय चुनावों में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते हैं। 21वीं सदी में स्वैच्छिक संगठन के कुछ नेता राजनीतिक दलों की मुख्यधारा में शामिल हुए, चुनाव लड़ा और कभी-कभार जीते भी, जैसे मधुसूदन मिस्त्री, जिन्होंने गुजरात से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में संसदीय चुनाव जीता था।
सूचना के अधिकार के लिए जन आंदोलन चलाने वाले तथा अरुणा राय के नेतृत्व वाले मजदूर किसान शक्ति संगठन (एमकेएसएस) ने राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों में अपने उम्मीदवार खड़े किए। इस संगठन को पहले से ही काफी समर्थन प्राप्त था इसलिए इसके उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई। हालांकि इसने एमकेएसएस के चुनावी आधार में आगे कोई इजाफा नहीं किया। स्थानीय सरकार में जमे रहने का निर्णय इस अनुभव से मिली सबसे बड़ी सीख है। शासन में पारदर्शिता के लिए एमकेएसएस द्वारा चलाया गया अभियान इसे समुदायों के और पास ले आया। स्थानीय सरकार के स्तर पर पार्टी से ज्यादा लोग मुद्दों से जुड़े तथा उम्मीदवारों और जनता के बीच सीधा संपर्क हुआ। इसलिए एमकेएसएस ने अपनी चुनावी रणनीति अच्छी तरह तैयार की।
पंचायतों में सफलता
भारत के सबसे बड़े जन आंदोलन, नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट (एनएपीएम) ने गंभीर वाद-विवाद के बाद वर्ष 2004 में चुनावी राजनीति में प्रवेश किया। अपने अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ लड़ने वाले विभिन्न समुदायों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए वर्ष 1992 में इस गठबंधन की स्थापना की गई थी। एनएपीएम स्वयं को दल-रहित राजनीतिक आंदोलन बताता है। वर्ष 2004 में इसने अलग पीपल्स पॉलिटिकल फ्रंट बनाया जो चुनाव लड़ सकता था। इसके जरिए एनएपीएम ने अपने दल-रहित छवि को बनाए रखा। यह फ्रंट दिल्ली-केंद्रित राजनीतिक दलों का विकल्प देने का वादा करता है।
एनएपीएम के संस्थापकों में से एक समाजवादी जन परिषद ने 1995 में स्वयं को राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत कराया। केजरीवाल के पूर्व सहयोगी योगेंद्र यादव इस पार्टी के सदस्य थे, हालांकि आम आदमी पार्टी से अलग होने के बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली है। उसने 2014 तक इस पार्टी के तहत चुनाव लड़ा और पंचायत, विधानसभा और संसदीय चुनावों में अपने प्रत्याशी खड़े किए। दलगत राजनीति से जुड़ने के लिए इसका तर्क था- इसने वर्षों तक स्थानीय समुदायों से जुड़े मुद्दों को तैयार किया, लेकिन चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों ने मुद्दों को हड़प लिया। चुनाव हो जाने के बाद, इन मुद्दों को भुला दिया गया जिससे फिर से आंदोलन की नौबत आ गई। जन परिषद ने विधानसभा और संसदीय चुनावों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया लेकिन पंचायत चुनावों में कुछ सफलता हासिल की।
उपर्युक्त प्रयोग दर्शाते हैं कि जन आंदोलन का चुनावी रूप स्थानीय सरकार के स्तर पर सफल रहा है। इन दलों के कई नेता उल्लेख करते हैं कि जन आंदोलनों के राजनीतिकरण ने अभी वह रूप नहीं लिया है जिससे वे विधानसभा और संसदीय चुनावों में प्रभाव डाल सकें, लेकिन पंचायतें उन्हें बेहतरीन अवसर प्रदान करती हैं क्योंकि इसमें स्थानीय मुद्दे शामिल होते हैं तथा नेताओं और मतदाताओं के बीच सीधा संपर्क होता है।
आम आदमी पार्टी ने इस प्रयोग को केवल संभावना के स्तर पर ही नहीं बल्कि चुनावी सफलता के स्तर पर भी विस्तार दिया है। यह सिविल सोसायटी का चुनावी पथ पर नया मोड़ है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कई लोकप्रिय वादे किए हैं, तथापि निर्णय लेने की प्रक्रिया में जनता को शामिल करना राजनीतिक दलों के लिए नया दौर है।
इस दृष्टिकोण से देखने पर हाल के आम चुनावों में सामाजिक कार्यकर्ताओं का चुनाव लड़ना एक महत्वपूर्ण बदलाव है। यह कहा जा रहा है कि इससे सिविल सोसायटी के कार्यकर्ताओं को सरकार के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इस टिप्पणी पर दो तरह से ध्यान देना जरूरी है। पहला, खुले तौर पर जाहिर न करने के बावजूद राजनीतिक दल सिविल सोसायटी के कार्यकर्ताओं के सैद्धांतिक झुकाव और राजनीतिक मत से परिचित होते हैं, चाहे वे चुनाव लड़ें या न लड़ें। चालाक राजनेता सामाजिक कार्यकर्ताओं से कथित गैर-साझेदार को तब तक स्वीकार करते हैं जब तक इससे उनका फायदा होता है। लुका-छुपी का यह खेल जारी रहने की उम्मीद है।
दूसरा, राजनेता चुनावों के जरिए अपने जनाधार और वैधता को साबित करने के लिए सिविल सोसायटी को चुनौती देते हैं। “अपनी धौंस दिखाकर” अब वे खुश हैं। चुनावों में कार्यकर्ताओं के खराब प्रदर्शन से राजनेताओं को भविष्य में उनकी मांग और विरोधों को अनदेखा करने का पर्याप्त औचित्य मिल सकता है। वास्तव में कार्यकर्ताओं की हार से सामाजिक आंदोलनों की सौदेबाजी की स्थिति को कमजोर होने के तौर पर देखा जा सकता है। पार्टिसिपेट्री रिसर्च इन एशिया (पीआरआईए) के राजेश टंडन कहते हैं, “मेरी नजर में, इसने सामाजिक और राजनीतिक कार्रवाई में अंतर को धुंधला कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप जनता की नजर में इससे कांग्रेस-समर्थक और भाजपा-समर्थक एनजीओ का नया वर्गीकरण हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ ऐसे जुड़ाव ने सामाजिक संगठनों को बांट दिया है। जो किसी भी दल से जुड़े नहीं हैं, उनके लिए आगे आने वाले समय में सामाजिक सुधार की स्वतंत्र कार्रवाई करने के अवसर सीमित होने की आशंका है।”
“इस चुनाव में स्थानीय मुद्दे रहेंगे हावी”कहने के लिए इस बार बालाकोट और राफेल डील की चर्चा हो रही है लेकिन इनसे ज्यादा बड़े मुद्दे नितांत स्थानीय हैं, इनमें किसानों से जुड़ा मुद्दा सबसे अधिक ज्वलंत है। यह देश के अलग-अलग हिस्सों में फैला हुआ हैसंभवत: ऐसा पहली बार होगा जब लोकसभा का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। कहने के लिए तो इस बार बालाकोट और राफेल डील की चर्चा है। लेकिन, इनसे ज्यादा बड़े मुद्दे नितांत स्थानीय हैं। जैसे, किसानों की कर्जमाफी, ग्रामीण इलाकों में रोजगार और विकास योजनाओं और खनन के कारण आदिवािसयों का विस्थापन आदि। ये ऐसे मुद्दे हैं, जो आमतौर पर मीडिया और अखबारों की सुर्खियां नहीं बनते हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में यही प्रमुख मुद्दे होने जा रहे हैं। हालांकि अभी इस पर सभी राजनीतिक दलों ने चुप्पी साध रखी है। इस बार देखा जाए तो देश भर में और विशेषकर हिंदी भाषी राज्यों के किसानों की कर्जमाफी का मुद्दा सबसे गरम है। इसकाे भुनाने की कोशिश कांग्रेस ने अभी से शुरू कर दी है। पंजाब का यदि उदाहरण देखें तो सत्ताधारी कांग्रेस की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार इसे अपना सबसे बड़ा चुनावी अस्त्र मान रही है। पिछले साल उसने दो लाख रुपए तक के कर्जदार छोटे और सीमांत किसानों के कर्ज माफ करने की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके बाद ही कांग्रेस तीन राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस मुद्दे को दोहराकर पिछले साल (2018) दिसंबर में सत्ता में लौट चुकी है। इसलिए पंजाब कांग्रेस इस मुद्दे पर अब एक कदम आगे बढ़ा रही है। कैप्टन ने नया वादा किया है कि पंजाब की आर्थिक स्थिति जैसे-जैसे मजबूत होगी, उसी अनुपात में किसानों के बड़े कर्ज भी माफ किए जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस अपनी इस सफल मुहिम को देश के अन्य राज्यों में भी इसी तरह आगे बढ़ाएगी। कहने का अर्थ कि एक राष्ट्रीय पार्टी का आगामी चुनाव में प्रमुख मुद्दा किसान होने जा रहा है। हालांकि भाजपा इसके तोड़ के रूप में कई राज्यों में ऐसे किसानों को सामने ला रहे हैं, जिन्हें कांग्रेस ने पोस्टर बॉय बनाया, लेकिन कर्ज माफ नहीं किया। ऐसे ही एक किसान को खड़ा कर अकाली दल ने लगभग दो लाख रुपए देकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश की तो कैप्टन ने सरकार को भी घेरा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी, 2019 को पंजाब में अपनी पहली सभा गुरदासपुर में की तो किसान कजर्माफी को धोखा बताया। यही बात वह तीन राज्यों में विधानसभा चुनावों के दौरान भी कह चुके थे। लेकिन उनकी बातों का असर उन राज्यों के मतदाताओं पर नहीं पड़ा। भाजपा बालाकोट एयर स्ट्राइक को भुनाकर देश भर में राष्ट्रवाद की लहर पैदा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका असर कहीं दिख नहीं रहा, कम से कम पंजाब जैसे सीमांत राज्य में तो नहीं। यह स्थिति तब है जब राज्य के लोग किसी भी सीमापार की लड़ाई में सबसे अधिक प्रभािवत होते हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश के अन्य राज्यों में क्या स्थिति होगी जबकि उनको सीमापार की जानकारी केवल मीडिया या टीवी के माध्यम से ही मिलती है। देश के शहरों में राष्ट्रवाद का मुद्दा जरूर उठाया जा रहा है। इस पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश हो रही है। खासकर कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ दोस्ती को विपक्ष मुद्दा बना रहा है। भाजपा के हर छोटे-बड़े नेता ने उन्हें कांग्रेस सरकार से बर्खास्त करने और पाकिस्तान भेज देने के बयान दिए। शायद यही कारण है कि 7 मार्च को मोगा में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की जब रैली हुई तो स्टार प्रचारक कहे जाने वाले नवजोत सिद्धू को बोलने का मौका नहीं दिया गया। ऐसे में माना यही जा रहा है कि पंजाब सहित राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस बार वोट बिल्कुल स्थानीय मुद्दों पर ही पड़ेंगे और कांग्रेस इन बड़े राज्यों में पिछले विधानसभा चुनाव जैसा प्रदर्शन दोहरा दे तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। किसानों के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड सहित देशभर के आदिवासी विकास परियोजनाओं से बेदखल किए जा रहे हैं। इस पर कोई भी राजनीतिक दल बोलने को तैयार नहीं दिख रहा है। जबकि हकीकत यह है कि देश में वनवासियों की संख्या लगभग 30 करोड़ से अधिक है। इस बार के चुनाव में ये जनसंख्या राष्ट्रीय दलों के लिए निर्णायक सािबत हो सकती है। क्योंकि इस ओर किसी राजनीतिक दल का ध्यान नहीं है। भाजपा तो जानबूझ कर इस मुद्दे को नहीं उठाएगी। आिखर इस मुद्दे पर उसे मुंह की ही खानी पड़ेगी। क्योंकि उसने तो आदिवासियों को जंगलों से ही बेदखल करने की योजना को अमलीजामा पहना िदया था। इस बार देश के धरतीपुत्र ही चुनाव का फैसला करने जा रहे हैं। |
यह लेख डाउन टू अर्थ, हिंदी के अप्रैल 2019 के अंक में प्रकाशित हो चुका है