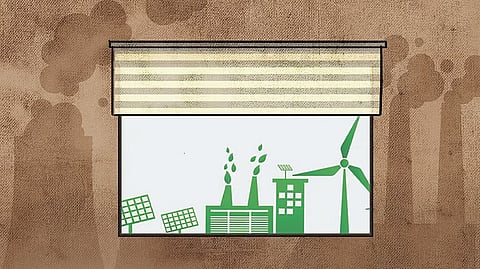स्वच्छ ऊर्जा: परिवर्तन की राह आसान बनाएं
हमारी दुनिया बदल चुकी है। यह जलवायु जोखिम का समय है और ट्रंप युग शुरू हो चुका है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने की दिशा में हुई कार्रवाई के खिलाफ पहले से ही विरोध चालू है और यह तब और भी बढ़ेगा जब धरती के बढ़ते तापमान का प्रभाव तीव्रता से दिखने लगेंगे।
अमीरों को बड़े पैमाने पर नुकसान सहना होगा और बीमाधारक इन आपदाओं से उबर पाने में सक्षम नहीं होंगे क्योंकि मूल्यों में लगातार वृद्धि और बीमा कंपनियों को विवश होकर बाजार छोड़ना होगा।
असली चुनौती समावेशी विकास और स्थिरता के सह-लाभों को एक साथ प्राप्त करना है। इसके साथ ही हमें डीकार्बोनाइजेशन के मार्ग पर भी बने रहना है क्योंकि यह हमारे जैसे “दक्षिण” के देशों के हित में है।
जीवाश्म ईंधन को स्वच्छ ऊर्जा में तब्दील करने के मुद्दे को ही लें। भारत में आज लाखों लोगों की आजीविका सुरक्षा के लिए उन्हें बिजली की सुविधा प्रदान करना एक अनिवार्य शर्त है। हमारे देश में आज भी ऐसे परिवार बड़ी संख्या में हैं जिनको भीषण ऊर्जा विपन्नता (एनर्जी पॉवर्टी) का सामना करना पड़ रहा है या तो उनको बिजली की सुविधा ही नहीं या अगर है भी तो महंगी और कब चली जाए उसका कोई भरोसा नहीं।
कई लोगों के लिए आज भी बिजली का बल्ब जलाना एक विलासिता है और महिलाएं गंदे बायोमास का प्रयोग कर खाना पकाने को विवश हैं। इससे उद्योग भी प्रभावित हुए हैं और यही वह समय है जब ऊर्जा की लागत आपकी प्रतिस्पर्धात्मकता को निर्धारित करती है।
यही कारण है कि भारतीय उद्योग कोयले जैसे ईंधन का उपयोग करके अपनी स्वयं की विद्युत उत्पादन प्रणाली (कैप्टिव पावर) को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए हमें अधिक ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा और सस्ती ऊर्जा इन तीनों के लिए रणनीति बनाने की आवश्यकता है।
यदि हम यह परिवर्तन सही तरीके से कर लेते हैं तो हम एक लो-कार्बन विकास की ओर बढ़ सकते हैं जो हमारे लिए तो कारगर होगा ही साथ ही साथ दुनिया को तबाही की ओर ले जाने वाले उत्सर्जन को कम करेगा।
यही कारण है कि केंद्र सरकार की 2030 तक 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन की योजना सराहनीय है। इस योजना में जानबूझकर कोयले को रिप्लेस अथवा प्रतिस्थापित (कोयला आज भारत के कुल बिजली उत्पादन के 75 प्रतिशत हिस्सा है) नहीं बल्कि इसे डिस्प्लेस (विस्थापित) करने की योजना बनाई गई है।
ऐसा सौर और पवन सहित स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की क्षमता को बढ़ाकर किया जाएगा और 2030 तक बिजली की मांग का 44 प्रतिशत इन स्रोतों से उत्पन्न करने का सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए स्वच्छ ऊर्जा को दोगुना से अधिक बढ़ाने की आवश्यकता होगी और संभव है कि इस अवधि में हमारे देश की बिजली की खपत भी दोगुनी हो जाए।
सरकार स्वच्छ ऊर्जा ट्रांजिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता को लेकर स्पष्ट रही है। हालांकि हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि इस दिशा में बहुत काम बचा है। हमें इस बात की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने की आवश्यकता है कि हमारे लिए क्या काम करता है और क्या नहीं।
भारत में आज लगभग 200 गीगावाट की स्थापित स्वच्छ ऊर्जा क्षमता है जो मार्च 2024 के हिसाब से देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 45 प्रतिशत है। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। इस अवधि में कुल बिजली के एक चौथाई से भी कम हिस्से का उत्पादन गैर-जीवाश्म स्रोतों से किया गया।
यदि आप केवल नए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (सौर-पवन) को देखेंगे जो कि ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें निवेश और स्थापना के मामले में साल-दर-साल प्रभावशाली वृद्धि देखी गई है तो यह आंकड़ा मात्र 13 प्रतिशत है। यह उस ऊर्जा परिवर्तन के अनुरूप नहीं है जिसकी हमें इतनी सख्त जरूरत है।
सरकार के अपने प्रस्ताव के अनुसार कोयले को “विस्थापित” करने के लिए 2030 तक कुल बिजली का लगभग 30 प्रतिशत उत्पादन स्वच्छ ऊर्जा के इन दो स्रोतों द्वारा किया जाना आवश्यक है।
क्या सौर व पवन की स्थापित और उत्पादन क्षमता के बीच बड़ा अंतर है? यदि हां तो क्यों? इस प्रश्न का उत्तर चालू संयंत्रों की कुल क्षमता के उपयोग कारक को ट्रैक करके ही मिलेगा। लेकिन यह आंकड़ा केवल केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के स्वामित्व वाले संयंत्रों के लिए उपलब्ध है और निजी पवन एवं सौर संयंत्रों के बारे में हम कुछ नहीं जानते।
दरअसल देश में चालू इकाइयों की संख्या, उनमें हो रहे बिजली के उत्पादन और उसे कहां बेचा या आपूर्ति किया जा रहा है इसका कोई सार्वजनिक डेटाबेस नहीं है। विडंबना यह है कि यह थर्मल पावर प्लांट के लिए तो यह जानकारी उपलब्ध है लेकिन नवीन ऊर्जा स्रोतों के लिए नहीं।
ऐसा लगता है कि निजी उद्योग निवेशकों द्वारा संचालित इस व्यवसाय में एक अनकहा समझौता है। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) की वेबसाइट से पता चलता है कि जून 2024 में प्रभावी बिजली खरीद समझौते (पीपीए अथवा पावर परचेज अग्रीमेंट) की तारीख के निकल जाने के बहुत समय बाद तक परियोजनाओं का एक बड़ा पोर्टफोलियो चालू नहीं हुआ था।
यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मौजूदा व्यवस्था के अंतर्गत परियोजनाओं को टेंडर तभी दिए जाते हैं जब पीपीए पर हस्ताक्षर हो जाते हैं यानी पहले से तय एक दर पर उत्पादित बिजली की खरीद पर सहमति बन जाती है।
यह भी तब किया जाता है जब परियोजना प्रस्तावक यह स्पष्ट कर देता है कि उसके पास परियोजना के लिए निवेश और जमीन सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। एसईसीआई के अनुसार ऐसी सौर, पवन और हाइब्रिड परियोजनाओं की कुल क्षमता 34.5 गीगावॉट तक है।
इसके अलावा 10 गीगावाट तक की परियोजनाएं अब भी पीपीए का इंतजार कर रही हैं। यह इसलिए अटकी हुई हैं क्योंकि राज्यों की बिजली खरीद एजेंसियां प्रस्तावित कीमत पर बिजली खरीदने के लिए राजी नहीं हैं। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब एक नई कोयला परियोजना से वितरित बिजली की लागत एक सौर परियोजना की तुलना में अधिक हो चुकी है।
एक कारण जो लगातार चर्चा में है वह यह है कि सूर्य और पवन ऊर्जा के अस्थायी स्रोत हैं। वे केवल तभी उपलब्ध होते हैं जब सूरज चमकता है और हवा चलती है। इसका उत्तर है कि ऐसी परियोजनाएं बनाई जाएं जिन्हें आमतौर पर चौबीसों घंटे चलने वाली (राउंड द क्लॉक) परियोजनाएं कहा जाता है।
जहां या तो बैटरी स्टोरेज या उच्च क्षमता के संयोजन से सुनिश्चित बिजली उत्पादन की व्यवस्था हो लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये परियोजनाएं भी अटक गई हैं और एसईसीआई के अनुसार वे अब तक चालू नहीं हुई हैं। भारत 500 गीगावाट स्वच्छ बिजली के अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, यह सुनिश्चित करने के लिए इन कमियों को ठीक करने की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण और आवश्यक दोनों है।