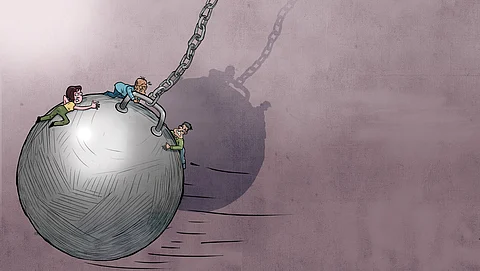
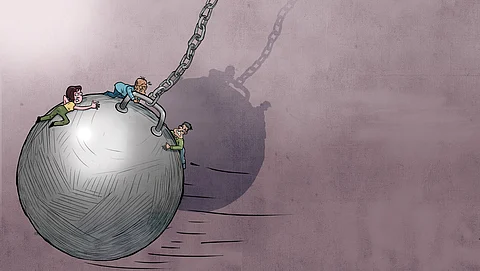
1,05,000 डॉलर, यह कीमत है द्वीप देश नाउरू के नागरिकता की। यह देश दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में सिर्फ 21 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह निचला द्वीप “गोल्डन पासपोर्ट” यानी नागरिकता बेचकर जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए धन जुटा रहा है। नाउरू दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश है और इसका वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में योगदान केवल 0.01 प्रतिशत है। फिर भी, यह देश समुद्र-स्तर में वृद्धि, तूफानी लहरों और तटीय कटाव से अस्तित्व के संकट का सामना कर रहा है। सरकार का कहना है कि उसके पास जलवायु संकट से खुद को बचाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं और नागरिकता बेचने से उसे द्वीप की 12,500 की कुल आबादी में से 90 प्रतिशत लोगों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बसाने और पूरी तरह एक नया समुदाय बसाने के लिए धन मिलेगा।
नाउरू की “गोल्डन पासपोर्ट” पहल यह दिखाती है कि दुनिया की 80 प्रतिशत आबादी वाले विकासशील देशों को दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर जलवायु संकट गहराता जा रहा है तो दूसरी ओर आर्थिक और वित्तीय कठिनाइयां भी बढ़ रही हैं। नतीजतन ये देश विदेशी ऋण पर निर्भर होते जा रहे हैं, जिससे वे जलवायु अनुकूलन और स्वच्छ ऊर्जा की ओर निवेश नहीं कर पा रहे हैं। इसके चलते वे आपदा से उबरने के लिए और अधिक उधार लेने को मजबूर हो जाते हैं और कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। इसका परिणाम तब और खतरनाक हो सकता है जब संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (यूएनटीडीएडी) की 2024 की रिपोर्ट यह चेता रही है कि 2023 में वैश्विक सार्वजनिक ऋण (यानि दुनिया भर की सरकारों का कुल उधार) रिकॉर्ड स्तर 97 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। इसका अर्थ है कि 2013 से 2023 के बीच व्यक्ति की औसत आय तो 22 प्रतिशत बढ़कर 13,065 डॉलर हो गई है, लेकिन उसी अवधि में व्यक्ति पर कर्ज का बोझ 61 प्रतिशत बढ़कर 12,034 डॉलर हो गया है। यह असमान वृद्धि काफी चिंताजनक है। क्योंकि इसका मतलब है कि व्यक्ति की आय का बड़ा हिस्सा अब कर्ज चुकाने में जा रहा है, जिससे देश जलवायु परिवर्तन और विकास लक्ष्यों पर निवेश नहीं कर पा रहे हैं। यह निवेश उनके राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (एनडीसी) के तहत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती और जलवायु प्रभावों के अनुकूलन के लिए आवश्यक है। जहां एक विकासशील देश (चीन को छोड़ कर) के एक नागरिक को जलवायु कार्रवाई के लिए साल 2030 तक हर साल लगभग 488 डॉलर की जरूरत है, वहीं इन देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सबसे अधिक खतरा है और उन्हें सबसे ज्यादा निवेश भी चाहिए।
यह हकीकत और भी गंभीर हो जाती है, जब इसे मौजूदा वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य के संदर्भ में देखा जाता है, खासकर तब जब विकसित देशों द्वारा विदेशी सहायता में कटौती की जा रही हो। अमेरिका का पेरिस समझौते से हटना जलवायु कार्रवाई को कमजोर करता है। अजरबैजान के बाकू में 2024 में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (कॉप29) में जलवायु वित्त पर नए सामूहिक लक्ष्य (एनसीक्यूजी) की बातचीत असफल रही, खासकर उन विकासशील देशों के लिए जो सार्वजनिक वित्त के जरिए जलवायु न्याय चाहते थे। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान चुपचाप नेट जीरो संधियों से पीछे हट रहे हैं और जलवायु वादों को सीमित कर रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड और स्वीडन जैसे बड़े दाता देश अपने विदेशी सहायता बजट में कटौती कर रहे हैं। ग्लोबल मैनेजमेंट कंसलटेंसी फर्म मैकिन्जे एंड कंपनी की मई 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, अगले वर्ष विदेशी सहायता में 22 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है। इसके अलावा, विकसित देशों से सार्वजनिक जलवायु वित्त अब भी जरूरत से बहुत कम है। अधिकांश ग्लोबल साउथ (विकासशील देशों) के लिए विकास और जलवायु वित्त का परिदृश्य निराशाजनक है। इस ठहराव की एक बड़ी वजह है बढ़ता बाहरी ऋण संकट, यानि कर्ज चुकाने के लिए और कर्ज लेना। सार्वजनिक ऋण की यह नई चिंता अब सामने आ रही है।
सॉवरेन डेट यानी सार्वजनिक ऋण का मतलब है कि केंद्रीय सरकार द्वारा विदेशी और घरेलू संस्थाओं से लिया गया कर्ज। यह कर्ज सरकारें कठिन परिस्थितियों का सामना करने और शिक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा जैसी सेवाओं में निवेश करने के लिए उधार लेती हैं। हालांकि, केंद्र द्वारा विदेशी मुद्रा में लिया गया बाहरी सार्वजनिक कर्ज दरअसल एक नई चिंता पैदा कर रहा है। यूएनसीटीएडी की 2024 की रिपोर्ट “ए वर्ल्ड ऑफ डेट: ए ग्रोविंग बर्डन टु ग्लोबल प्रॉसपेरिटी” में कहा गया है, “सार्वजनिक ऋण विकास का एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, जो सरकारों को महत्वपूर्ण खर्च करने और लोगों के लिए बेहतर भविष्य में निवेश करने में सक्षम बनाता है।” लेकिन जब यह ऋण बहुत अधिक या तेजी से बढ़ता है तो यह विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए भारी बोझ बन जाता है।
रिपोर्ट के अनुसार, हाल के वर्षों में कई संकटों और वैश्विक अर्थव्यवस्था के असमान प्रदर्शन के कारण वैश्विक सार्वजनिक ऋण में खतरनाक वृद्धि हुई है। 2023 में यह 97 ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष से 5.6 ट्रिलियन डॉलर अधिक था। हालांकि विकसित देश दो-तिहाई सार्वजनिक ऋण के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन निम्न और मध्यम आय वाले विकासशील देशों पर भी 29 ट्रिलियन डॉलर का ऋण है।
चिंता की बात यह है कि 2010 से अब तक विकासशील देशों में सार्वजनिक ऋण दोगुनी गति से बढ़ा है, जिससे 2010 में इनका हिस्सा वैश्विक ऋण में 16 प्रतिशत था, जो 2023 में 30 प्रतिशत हो गया है। इन देशों के ऋण का एक बड़ा हिस्सा बाहरी (विदेशी) ऋण है। यानि विदेशी कर्जदाता से लिया गया पैसा । यह विदेशी मुद्रा भंडार को धीरे-धीरे समाप्त करता है और जब घरेलू मुद्रा कमजोर होती है, तो कर्ज लौटाना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई देश विदेशी मुद्रा में कर्ज चुकाने की क्षमता खो देता है, तो बाहरी ऋण आर्थिक संकट ला सकता है। श्रीलंका और केन्या जैसे देश इसका खामियाजा भुगत चुके हैं, जहां अस्थिर बाहरी ऋण के कारण संकट और सामाजिक असंतोष पैदा हुआ।
जर्नल ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में फरवरी 2024 में प्रकाशित विश्लेषण “व्हाट ब्रोक द पर्ल ऑफ इंडियन ओशियन?” के मुताबिक, श्रीलंका में संकट का मुख्य कारण था बजट घाटे को विदेशी उधारी से पूरा करना। 2018 तक उसका बाहरी ऋण केंद्र सरकार के कुल ऋण का 50 फीसदी हो गया था ,जो 20 वर्षों में सबसे ज्यादा था। वहीं, 2020 में, जब कोविड-19 महामारी आई, तो विदेश से कर्ज आना बंद हो गया। सरकार ने चालू खाता घाटा पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल किया। लगातार भंडार खत्म होने के कारण, श्रीलंका अप्रैल 2022 में अपने बाहरी कर्ज पर चूक कर गया। इससे पूरी अर्थव्यवस्था और देश ठप पड़ गया और सामाजिक-राजनीतिक संकट शुरू हो गया।
विश्व बैंक के आंकड़े दिखाते हैं कि कई और विकासशील देशों की हालत भी चिंताजनक है। 2013 से 2023 के बीच इन देशों का बाहरी ऋण 55 प्रतिशत बढ़ा। यानी 5.71 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 8.84 ट्रिलियन डॉलर हो गया। इनका सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) यानी देश के नागरिकों की कुल आमदनी भी 52 प्रतिशत बढ़ी, लेकिन कर्ज की गति अधिक रही (देखें, बढ़ता बाहरी ऋण बोझ)। इन ऋणों का अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र ने लिया है। यानी सरकार और सरकारी संस्थाओं से। यह दर्शाता है कि यह ऋण आवश्यक बजटीय जरूरतों को पूरा करने के लिए लिया गया।
क्षेत्रीय विश्लेषण बताता है कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र पिछले दस वर्षों में वैश्विक दक्षिण के भीतर सरकार-स्वामित्व वाले बाहरी ऋण का सबसे बड़ा बोझ उठाता रहा है। 2013 से 2023 के बीच इस क्षेत्र का ऋण 829 बिलियन डॉलर से बढ़कर 1.63 ट्रिलियन डॉलर हो गया। वहीं, अगर चीन को छोड़ दें, जो अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक ऋण वाला देश है और खुद एक बड़ा कर्जदाता भी है, उस पर 1.7 गुना ऋण बढ़ा है। यानी यह 676.7 बिलियन डॉलर से बढ़कर 1.16 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है। लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों का ऋण 574 बिलियन डॉलर से 940 बिलियन डॉलर (1.6 गुना) बढ़ा है। अफ्रीका में यह दोगुना हो गया है। यहां 2023 में 689 बिलियन डॉलर था। अब और अधिक देशों को उच्च ऋण बोझ का सामना करना पड़ रहा है, इसमें विशेष रूप से अफ्रीका शामिल है (देखें, स्पष्ट क्षेत्रीय अंतर,)।
साल 2010 से अब तक विकासशील देशों पर सार्वजनिक (सॉवरेन) ऋण विकसित देशों की तुलना में दो गुना तेजी से बढ़ा है। और वैश्विक ऋण में इसका हिस्सेदारी 2010 के 16 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 30 प्रतिशत हो गई है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर विकासशील देश तेजी से कर्ज के बोझ तले क्यों दबते जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब अक्सर 1970 के दशक में तेल की कीमतों में आई भारी वृद्धि से जोड़ा जाता है। तेल आयात करने वाले विकासशील देशों के लिए यह स्थिति एक बड़े वित्तीय संकट जैसी बन गई थी। उस दौर में अरब देशों की तेल से हुई कमाई (पेट्रोडॉलर) पश्चिमी देशों के बैंकों में जमा हो गई। यही पेट्रोडॉलर बाद में विकासशील देशों को दिए गए कर्ज का प्रमुख स्रोत बने। यह व्यवस्था पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी फायदेमंद थी। जब तेल से कमाया गया पैसा विकासशील देशों को कर्ज के रूप में वापस दिया गया, तो वे देश तेल के बढ़े हुए बिल के बावजूद पश्चिमी देशों से सामान खरीदते रहे। इससे यूरोप और उत्तर अमेरिका की फैक्ट्रियां चालू रहीं और वहां मंदी आने से टल गई। 1970 के दशक के दौरान पश्चिमी देशों के निजी वाणिज्यिक बैंकों ने धीरे-धीरे सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। 1982 में जब ये बैंक अपने चरम पर थे, तब वे विकासशील देशों को हर साल 63 अरब डॉलर का कर्ज दे रहे थे, जो कि सरकारी स्रोतों से दिए जा रहे ऋण की लगभग दोगुनी राशि थी। इस दौर में कई विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएं तेजी से बढ़ रही थीं। लेकिन 1980 का दशक औद्योगिक देशों में आई आर्थिक मंदी के लिए जाना गया। उत्पादन और व्यापार की गतिविधियां धीमी हो गईं, और बैंकों के कर्ज पर ब्याज दरें तेजी से बढ़ गईं। ऐसे में जिन विकासशील देशों के पास पहले से लिए गए कर्ज चुकाने के लिए संसाधन नहीं थे, वे सिर्फ ब्याज चुकाने के लिए ही नया कर्ज लेने पर मजबूर हो गए। आइए अब सीधा 2020 के दशक में लौटते हैं। पिछले 40 सालों में हालात ज्यादा नहीं बदले हैं।
विश्व बैंक की इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट (दिसंबर 2024) के अनुसार, विकासशील देशों ने 2023 में अपनी बाहरी (विदेशी) ऋण की सेवा यानी कर्ज पर ब्याज और किस्त चुकाने के लिए रिकॉर्ड 1.4 ट्रिलियन डॉलर खर्च किए। यह खर्च इसलिए भी बढ़ा क्योंकि उस साल ब्याज दरें 20 वर्षों के उच्चतम स्तर पर थीं। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) की रिपोर्ट “ए वर्ल्ड ऑफ डेट” में बताया गया, “वर्तमान में आधे से अधिक विकासशील देश अपने कुल सरकारी राजस्व का कम से कम आठ प्रतिशत केवल ब्याज भुगतान पर खर्च कर रहे हैं, जो पिछले दशक में दोगुना हो चुका है। ब्याज चुकाने का यह बढ़ता दबाव लगभग सभी क्षेत्रों में महसूस किया जा रहा है, लेकिन अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों में स्थिति विशेष रूप से गंभीर है।” साल 2023 में 54 विकासशील देशों (जो कुल का 38 प्रतिशत हैं) ने सरकारी राजस्व का 10 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सा ब्याज भुगतान में खर्च किया, जो एक रिकॉर्ड है। इन देशों में से लगभग आधे अफ्रीका में हैं। विकासशील देशों में ब्याज भुगतान न केवल तेजी से बढ़ रहा है, बल्कि यह जनहित से जुड़े आवश्यक सरकारी खर्च की वृद्धि को भी पीछे छोड़ रहा है। 2023 में दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की रिपोर्ट “बियॉन्ड क्लाइमेट फाइनेंस” में यह बताया गया कि कई निम्न और मध्यम आय वाले देश (एलएमआईसी) कर्ज चुकाने में जितना खर्च कर रहे हैं, वह उनकी जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने की अनुमानित लागत से भी अधिक है। एलएमआईसी सरकारों का सालाना बाहरी ऋण भुगतान 2013 में 182 अरब डॉलर था, जो 2023 में दोगुना बढ़कर 368 अरब डॉलर हो गया (देखें, बेहद असहज स्तर पर पहुंचा कर्ज बोझ)। यह स्थिति तब साफ होती है जब देखा जाए कि किसी देश द्वारा अर्जित प्रति डॉलर सकल राष्ट्रीय आय प्रति डॉलर (जीएनआई) में से कितना हिस्सा बाहरी सार्वजनिक ऋण चुकाने में जाता है। 2013 में एक विकासशील देश औसतन 1.6 सेंट (1.6 फीसदी) खर्च करता था, जो 2023 में बढ़कर 2.5 सेंट हो गया। एलएमआईसी देशों में यह खर्च 1.8 सेंट से बढ़कर 2.8 सेंट पहुंच गया।
कर्ज चुकाने की लागत इतनी अधिक होने का एक प्रमुख कारण है कि उधार देने वाले देश बहुत अधिक ब्याज वसूल रहे हैं। यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट में दिखाया गया है कि विकासशील देश उन दरों पर उधार लेते हैं जो अमेरिका की तुलना में दो से चार गुना अधिक और जर्मनी की तुलना में छह से 12 गुना अधिक होती हैं। रिपोर्ट के अनुसार, “इस ऋण का बोझ अलग-अलग देशों पर अलग तरह से पड़ता है और इसे चुकाने की क्षमता उस असमानता से और जटिल हो जाती है जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना में अंतर्निहित है।” ऐसा मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि विकासशील देशों को आम तौर पर “उच्च जोखिम वाला क्षेत्र” माना जाता है, जिसके चलते उन्हें उधार लेने के लिए अधिक लागत चुकानी पड़ती है। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स किसी देश की कर्ज चुकाने की क्षमता का स्वतंत्र मूल्यांकन मानी जाती हैं। ये रेटिंग्स इसलिए महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि वैश्विक वित्तीय बाजार में इन्हीं के आधार पर किसी देश के लिए ब्याज दरें तय होती हैं और इस तरह उसकी उधारी की लागत पर सीधा असर पड़ता है। दुर्भाग्य से, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स में ग्लोबल साउथ के देशों के प्रति पूर्वाग्रह देखा गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की 2023 की रिपोर्ट, “रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फाइनेंस फॉर अफ्रीका” के अनुसार, असमान रेटिंग्स के कारण अफ्रीकी देशों को 24 अरब डॉलर से अधिक अतिरिक्त ब्याज चुकाना पड़ा है और 46 अरब डॉलर से अधिक की संभावित उधारी गंवानी पड़ी है।
उदाहरण के लिए, अमेरिका की स्टॉकटन यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र और वैश्विक अध्ययन की प्रोफेसर राम्या विजया ने मार्च 2025 में दानिश डेवलपमेंट रिसर्च नेटवर्क को दिए एक साक्षात्कार में कहा, कैमरून और इथियोपिया की क्रेडिट रेटिंग उस समय घटा दी गई, जब उन्होंने डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव के तहत राहत की मांग की। यह पहल जी20 देशों द्वारा मई 2020 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव से जूझ रहे निम्न और निम्न-मध्यम आय वाले देशों को सहायता देना था। लेकिन इन देशों की रेटिंग घटा दिए जाने से उनके कर्ज की लागत बढ़ गई, जिससे उनके बजट पर बोझ और बढ़ा और आर्थिक पुनरुद्धार की प्रक्रिया लंबी खिंच गई। उन्होंने सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स और विकासशील देशों के लिए वित्त तक असमान पहुंच के व्यापक प्रभावों पर चर्चा करते हुए कहा कि यह बेहद जरूरी है कि हम देश रेटिंग्स के दीर्घकालिक प्रभावों की जांच करें, क्योंकि यही तय करता है कि सरकारें, खासकर ग्लोबल साउथ के वे देश जिनकी कर आय कम होती है, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास से जुड़े अन्य अहम क्षेत्रों पर कितना खर्च कर सकती हैं।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ ) की एक रिपोर्ट के अनुसार, ग्लोबल नॉर्थ देशों ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए औसतन अपनी जीडीपी का 12 प्रतिशत खर्च किया। इसके मुकाबले, उभरती अर्थव्यवस्थाओं (विकासशील देशों) ने 6 प्रतिशत और निम्न-आय वाले देशों ने सिर्फ 3 प्रतिशत खर्च किया। फिर भी 2020 में सॉवरेन रेटिंग में गिरावट के 95 प्रतिशत मामले उभरते और विकासशील देशों के हिस्से में आए।
यह दिखाता है कि विकसित देशों को रेटिंग एजेंसियों की ओर से अतिरिक्त छूट मिलती है ताकि वे मंदी के दौरान खर्च बढ़ा सकें या टैक्स घटा सकें जिससे आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन दिया जा सके। इस कारण, ऐसे देश संकटों से तेजी से उबर जाते हैं। वहीं, ग्लोबल साउथ के देश रेटिंग गिरने के डर से सरकारी खर्च नहीं बढ़ा सकते, जिससे उनके लिए संकट से उबरना और मुश्किल हो जाता है। इस तरह की प्रो-साइक्लिकल नीतियां यानी अर्थव्यवस्था में जब मंदी हो तो खर्च में कटौती और जब तेजी हो तो खर्च में बढ़ोतरी जैसी नीतियां कर्ज की समस्या को और भी बढ़ा देती हैं। यह भी देखा गया है कि अफ्रीका में सॉवरेन कर्ज पर ब्याज भुगतान में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, जो 2013 में 7.8 अरब डॉलर से बढ़कर 2023 में 25.1 अरब डॉलर हो गया, यानी 3.2 गुना की बढ़ोतरी।
एशिया और पैसिफिक क्षेत्र में भी यही रुझान देखने को मिला, जहां सॉवरेन ऋण पर ब्याज भुगतान 2013 के 20.9 अरब डॉलर से बढ़कर 2023 में 64.1 अरब डॉलर हो गया, जो तीन गुना से अधिक है और साल 2023 में कुल वैश्विक ब्याज भुगतान का सबसे बड़ा हिस्सा (48.7 प्रतिशत) भी यही क्षेत्र रहा। लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र में यह वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी रही, जहां ब्याज भुगतान 1.6 गुना बढ़ा।
विकसशील देशों पर चढ़ता कर्ज बोझ अब उस स्थिति तक पहुंच चुका है जहां उत्तर से दक्षिण की ओर संसाधनों का प्रवाह पूरी तरह उलट गया है। वर्ल्ड बैंक के आंकड़े बताते हैं कि जब विकासशील देश सबसे ज्यादा आर्थिक तंगी में थे, तभी उन्होंने अपने विदेशी कर्जदाताओं से जितना नया कर्ज मिला था, उससे करीब 38.5 अरब डॉलर ज्यादा वापस चुका दिया (देखें, वास्तव में कितना आता है)। यानी 2022 और 2023 में इन देशों से पैसा बाहर गया, अंदर नहीं आया। कुल मिलाकर जो मदद मिलनी चाहिए थी, उसके उलट उन्होंने अमीर देशों को ही ज्यादा पैसा दे दिया। कोई अन्य आंकड़ा इस बात का ज्यादा क्रूर मजाक नहीं हो सकता कि अमीर देश खुद को विकासशील देशों के मददगार के रूप में देखते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह संसाधनों का उलटा प्रवाह केवल अनैतिक नहीं है, बल्कि यह गरीब देशों में जारी गरीबी और पर्यावरणीय क्षरण का प्रमुख कारण भी है, जहां आर्थिक संसाधनों का तेजी से दोहन केवल इसलिए किया जाता है ताकि कर्ज चुकाया जा सके।
अगर कर्ज वित्त प्रवाह का समग्र मूल्यांकन करें तो उधार देने वाले और विकासशील देशों के बीच जो प्रवृत्ति बन रही है वह चिंताजनक है। सार्वजनिक कर्ज पर शुद्ध प्रवाह का मतलब है किसी वर्ष में कुल देनदारियों से मिलने वाला ऋण और उसके बदले देनदार देश द्वारा मूलधन और ब्याज में किया गया भुगतान। अगर किसी वर्ष यह आंकड़ा ऋणदाता के पक्ष में निगेटिव होता है तो इसका अर्थ है कि कर्जदार देश ने कर्ज के रूप में जितना पैसा प्राप्त किया, उससे कहीं ज्यादा भुगतान कर दिया।
दुनिया का तीसरा सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता नीदरलैंड्स ने 2023 में निम्न और मध्यम-आय वाले देशों (एलएमआईसीएस) को 9.9 अरब डॉलर का बाह्य सार्वजनिक ऋण दिया, लेकिन उससे 17.02 अरब डॉलर की वसूली की। इसका अर्थ है कि वहां से 7.12 अरब डॉलर का ऋण शुद्ध रूप में आया। इसी तरह, दुनिया के सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता चीन ने 2023 में एलएमआईसीएस को 12.07 अरब डॉलर का ऋण दिया, लेकिन बदले में 24.14 अरब डॉलर की वसूली की। यह 12 अरब डॉलर का ऋणात्मक शुद्ध प्रवाह दर्शाता है।
अक्सर ऋणदाता देशों द्वारा ऐसे ऋण समझौते किए जाते हैं जिनमें देश की प्राकृतिक संसाधनों की निर्यात आय को ऋण भुगतान से जोड़ दिया जाता है।
2015 से लगातार निम्न-आय वाले देशों में सकल पूंजी निर्माण (अर्थव्यवस्था की स्थायी परिसंपत्तियां जैसे स्कूल, अस्पताल और कारखाने) जीडीपी का मात्र 22 प्रतिशत बना हुआ है, जो मध्य-आय वाले देशों के 33 प्रतिशत के औसत से काफी कम है। यह जानकारी वैटिकन समर्थित द जुबली रिपोर्ट में दी गई है। इस रिपोर्ट को पोप फ्रांसिस के आदेश पर 30 प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने तैयार किया है। गरीबी से उबर चुके और मध्य आय वाले देशों की बराबरी करने के लिए निम्न-आय वाले देशों को अपने जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा निवेश करना चाहिए।
बढ़ते हुए सरकारी कर्ज की अदायगी और उसके कारण देश की वित्तीय सेहत पर पड़ने वाला बोझ चिंता पैदा करने वाला है। जीडीपी के अनुपात में बाहरी सार्वजनिक ऋण भुगतान की तुलना यदि सरकार के स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च के अनुपात से की जाए तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आते हैं।
पिछले एक दशक में ऐसे देशों की संख्या में 47 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है, जहां बाहरी ऋण भुगतान स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च को पीछे छोड़ रहा है। 2013 में नौ देशों में बाहरी सार्वजनिक ऋण के भुगतान का जीडीपी में हिस्सा, शिक्षा पर सरकारी खर्च के जीडीपी में हिस्से से अधिक था। वहीं, 35 देशों का बाह्य ऋण भुगतान का हिस्सा स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च से अधिक था। 2023 तक यह संख्या बढ़कर 17 और 48 हो गई।
इसके अलावा 2023 में 11 देशों में विदेशी सार्वजनिक ऋण भुगतान का जीडीपी में हिस्सा शिक्षा पर सरकारी खर्च के जीडीपी में हिस्से से 1 प्रतिशत अंक से भी अधिक था। इंडोनेशिया के मामले में यह अंतर 2.1 प्रतिशत था, मालदीव में 5.1 प्रतिशत, अंगोला में 5.9 प्रतिशत, जबकि मंगोलिया में यह अंतर 8.2 प्रतिशत तक पहुंच गया। इसी तरह 21 देशों में बाहरी ऋण भुगतान का जीडीपी में हिस्सा, स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च के जीडीपी में हिस्से से 1 प्रतिशत अंक से अधिक था। इनमें से 13 देशों में यह अंतर 2 प्रतिशत अंक से भी अधिक था। उदाहरण के लिए, इंडोनेशिया में यह अंतर 1.6 प्रतिशत, कैमरून में 3 प्रतिशत, कांगो में 4.7 प्रतिशत, जॉर्डन में 4.9 प्रतिशत और अंगोला में 6.4 प्रतिशत था। इससे पता चलता है कि ग्लोबल साउथ में विकास पर किए जा रहे खर्च में अस्थिरता बहुत, जिसका कारण बढ़ता सार्वजनिक ऋण संकट है।
अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संस्था एक्शनएड की 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार बढ़ता कर्ज देशों को एक नकारात्मक चक्र में फंसा रहा है, जिसके कारण सरकारों को न केवल स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं पर खर्च कम करना पड़ रहा है, बल्कि उन्हें अपने ऋण चुकाने के लिए उन क्षेत्रों में निवेश करना पड़ रहा है जो जलवायु के लिहाज से हानिकारक हैं। घाना जैसे देश अपना ऋण चुकाने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे अहम क्षेत्रों में फंडिंग में कटौती कर रहे हैं (देखें, कर्ज का चक्रव्यूह)।
विकासशील देशों के लिए कर्ज और जलवायु संकट अब एक साथ गहराते जा रहे हैं और यह मिलकर एक दुष्चक्र बना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) और यूनाइटेड किंगडम की स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जलवायु परिवर्तन ने पहले ही विकासशील देशों के लिए कर्ज की औसत लागत को 117 बेसिस पॉइंट तक बढ़ा दिया है। एक बेसिस पॉइंट का मतलब है 0.01 प्रतिशत यानी विकासशील देशों को 1.17 प्रतिशत ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ रहा है। यह अंतर मामूली नहीं है क्योंकि अरबों डॉलर के कर्ज पर यह एक बड़ी राशि बन जाता है। कई सबसे संवेदनशील देशों के लिए जलवायु परिवर्तन से निपटने की लागत दरअसल उन क्षति लागतों के बराबर हो गई है जो जलवायु से प्रेरित या और बदतर हुए मौसमीय हादसों से जुड़ी हैं। मसलन, डोमिनिका और अन्य कैरेबियाई देशों पर भारी कर्ज का मुख्य कारण पहले आए तूफान रहे हैं। 2015 में जब डोमिनिका पर एरिका नाम का तूफान आया तब कुल नुकसान देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 90 प्रतिशत तक पहुंच गया था। हाल के वर्षों में समुद्र स्तर बढ़ने के खतरे का सामना कर रहे कई छोटे द्वीपीय देशों ने जलवायु संकट के भौतिक और आर्थिक प्रभावों के बीच कर्ज माफी की मांग को लेकर एकजुटता के साथ आवाज उठाई है।
वहीं, कम और मध्यम आय वाले देशों में से जो जलवायु के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं, उनमें से आधे से ज्यादा देश या तो पहले से ही कर्ज संकट में हैं या फिर उसके बहुत करीब हैं। ऐसे 36 देश हैं, जो या तो कर्ज संकट से जूझ रहे हैं या फिर उसके कगार पर हैं (देखें, हर कोने से खतरा,)।
इनका अनुभव यह दिखाता है कि कैसे कर्ज का बोझ उनके लिए वित्तीय गुंजाइश को घटा देता है, जलवायु जोखिम को और गहरा करता है और अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त इस असंतुलन को दूर करने के लिए अब भी अपर्याप्त है। विकासशील देशों को जलवायु कार्रवाई के लिए ज्यादा और व्यापक वित्तीय मदद की जरूरत है। जो देश जलवायु और आर्थिक दोनों तरह के झटकों के प्रति सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं उन्हें ऐसा जलवायु वित्त चाहिए जो कर्ज सरीखा न हो। यानी कर्ज रहित वित्त। इस विश्लेषण में शामिल 40 देशों को 2012 से 2022 के बीच 78 अरब डॉलर का विकास वित्त मिला जिसमें जलवायु संबंधी कुछ तत्व शामिल थे। हालांकि यह एक उदार अनुमान है क्योंकि कई बार परियोजनाओं के स्तर पर जलवायु की भूमिका स्पष्ट नहीं होती और ऊपर से यह आंकड़ा कर्ज देने वाले देशों द्वारा घोषित वादों पर आधारित होता है। वास्तविक भुगतान अक्सर अलग होता है। पहले भी यह बात सामने आई है कि जलवायु वित्त की राशि दरअसल विकास वित्त की तुलना में बहुत कम अंश में वितरित होती है। कई बार तो यह आधी से भी कम होती है।
हर साल की औसत से देखें तो इन 40 देशों को सालाना 7.17 अरब डॉलर मिले। वहीं दूसरी ओर, इन देशों की राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं को लागू करने की वार्षिक आवश्यकता 79 अरब डॉलर है। यह अंतर काफी बड़ा है। इसी बीच जलवायु से जुड़ी आपदाओं से होने वाले नुकसान लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जब हम इस परिप्रेक्ष्य में सार्वजनिक कर्ज की स्थिति को भी जोड़ते हैं, तो तस्वीर और ज्यादा गंभीर हो जाती है।
ये देश या तो पहले से ही कर्ज संकट में हैं या उसके बेहद करीब हैं। वर्ल्ड बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) कर्ज संकट को उस स्थिति के रूप में परिभाषित करते हैं जब कोई देश अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ हो जाए और कर्ज का पुनर्गठन जरूरी हो जाए। अगर कोई देश संप्रभु कर्ज में चूक करता है, तो उसे बाजार तक पहुंच खोनी पड़ती है और उसे और भी ज्यादा ब्याज दरों पर कर्ज मिल सकता है। 2022 में ही इन 36 देशों ने कुल 13.24 अरब डॉलर बाहरी संप्रभु कर्ज के भुगतान में खर्च कर दिए। यह उस राशि का 1.8 गुना है जो उन्हें साल भर में जलवायु संबंधी विकास वित्त के रूप में मिली। यानी उन्होंने जलवायु कार्रवाई के लिए जो कुछ मिला, उसका लगभग दोगुना केवल कर्ज चुकाने में लगा दिया।
इन 36 देशों में से एक-तिहाई ऐसे हैं जो जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं और सबसे कम तैयार भी। जब हम इनके जलवायु वित्त की जरूरतों और प्राप्त फंड व सार्वजनिक कर्ज सेवा को एक साथ देखते हैं तो पता चलता है कि इन देशों को वित्तीय सहायता तो कम मिलती है लेकिन कर्ज चुकाने का बोझ बहुत भारी है। यहां तक कि कई बार शिक्षा या स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च से भी ज्यादा। हर देश की स्थिति अपनी जगह खास है, लेकिन यह तस्वीर पूरे वैश्विक वित्तीय तानेबाने में मौजूद विषमता को उजागर करती है।
ज्यादातर देशों में जो पैसा कर्ज सेवा में जा रहा है, वह या तो उन्हें मिले जलवायु वित्त से ज्यादा है या उनके जीडीपी के अनुपात में सामाजिक सेवाओं पर खर्च से भी। उदाहरण के लिए चाड, गिनी-बिसाउ, हैती और सिएरा लियोन जैसे देशों में कर्ज सेवा पर खर्च उस रकम से ज्यादा है जो उन्हें जलवायु-संबंधी विकास सहायता के रूप में मिली। अफ्रीकी देश चाड और गिनी-बिसाउ व कैरिबियाई देश हैती में यह खर्च सामाजिक व्यय से भी ज्यादा है। इस अध्ययन में शामिल 36 देशों में से 25 के लिए जलवायु आपदाओं से हुए नुकसान के विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध थे। इन 25 में से करीब 70 प्रतिशत ने 2022 में जितना पैसा सार्वजनिक कर्ज सेवा में दिया, वह जलवायु आपदाओं से हुई सालाना औसत क्षति से भी ज्यादा था। इनमें से जाम्बिया, घाना, कैमरून और ताजिकिस्तान, कुल चार देश ऐसे से थे जहां सार्वजनिक कर्ज सेवा, जलवायु से हुए नुकसान से 50 गुना ज्यादा थी। इसमें आश्चर्य नहीं कि इनमें से घाना और जाम्बिया, ने अपने बाहरी कर्ज को फिर से संरचित करने की कोशिश की लेकिन उन्हें बहुत सीमित सफलता मिली। भले ही जलवायु से जुड़े नुकसान समय-समय पर होते हैं और कर्ज सेवा एक नियमित जिम्मेदारी होती है लेकिन इस तुलना से यह स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह सार्वजनिक धन का ढांचा असंतुलित है। इसका मतलब यह है कि किसी देश के पास जलवायु आपदा से निपटने से पहले ही वित्तीय संसाधन काफी हद तक ऋणदाताओं को देने के लिए आरक्षित होते हैं और यह आरक्षण आपदा से होने वाले औसत नुकसान से कहीं ज्यादा होता है। ऐसे में जब असली जलवायु संकट आता है, तब कोई उपाय करने की गुंजाइश नहीं बचती। यह तुलना ये बताने के लिए नहीं है कि दोनों बराबर हैं बल्कि यह इस सच्चाई को उजागर करने के लिए है कि किस तरह सख्त और एकतरफा वित्तीय जिम्मेदारियां दरअसल किसी देश की तैयारी और संभलने की ताकत को पूरी तरह बाधित कर सकती हैं जबकि जलवायु संकट अप्रत्याशित और विनाशकारी होता है।
विकासशील देशों में बढ़ते कर्ज संकट को अक्सर वित्तीय अनुशासनहीनता या शासन की विफलता के रूप में पेश किया जाता है। लेकिन हाल ही में जारी “द जुबिली रिपोर्ट” यह दिखाती है कि यह धारणा न केवल भ्रामक है बल्कि अधूरी भी है। सच्चाई यह है कि आज का संकट वैश्विक वित्तीय व्यवस्था, ऋणदाताओं के व्यवहार और सुनियोजित उपेक्षा की एक प्रणालीगत विफलता है। कर्ज लेने वाली सरकारों ने अक्सर अपनी क्षमता से ज्यादा और खराब शर्तों पर कम अवधि वाले कर्ज लिए, भले ही ऋण देने वाले निजी निवेशक हों या बहुपक्षीय संस्थाएं। हमेशा बेहतर मुनाफे की लालच में जानते-बूझते जोखिम भरा और अत्यधिक कर्ज देते रहे। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं ने इस संकट को और गहरा किया क्योंकि उन्होंने कठिन सवालों से बचने की कोशिश की और केवल अस्थायी समाधान दिए। साथ ही एक ऐसी व्यवस्था को बनाए रखा जो दीर्घकालिक स्थिरता की बजाय अल्पकालिक लाभ को तरजीह देती हैं।
इस पूरे संकट की जड़ में एक बड़ी खामी है। दुनिया की आर्थिक व्यवस्था में ऐसा कोई अंतरराष्ट्रीय ढांचा ही नहीं है जो देशों के कर्ज संकट से ठीक से निपट सके। अगर कोई कंपनी दिवालिया होती है तो उसके पास खुद को दोबारा व्यवस्थित करने का रास्ता होता है। लेकिन जब कोई देश संकट में होता है तब उसे अलग-अलग, बिखरे हुए और ऋणदाताओं के दबदबे वाली बातचीत की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जहां न तो कोई तय समयसीमा होती है, न ही न्याय और बराबरी की गारंटी। इसी बीच, वैश्विक वित्तीय व्यवस्था की गहरी असमानताएं और भी चौड़ी होती जा रही हैं।
अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों का सार्वजनिक कर्ज अब उनकी जीडीपी के 100 प्रतिशत से ज्यादा हो चुका है, बावजूद इसके इन देशों को ऐसा कर्जदार माना जाता है जो पैसा लौटाने में भरोसेमंद है, इसलिए उन्हें कर्ज भी आसानी और सस्ते ब्याज पर मिल जाता है। वहीं, जिम्बाब्वे और चाड जैसे देश, जिनका कर्ज से जीडीपी अनुपात काफी कम है उन्हें बेहद ऊंची ब्याज दरों और कठोर शर्तों का सामना करना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि समृद्ध देश आमतौर पर अपनी मुद्रा में कर्ज लेते हैं, उन्हें उच्च क्रेडिट रेटिंग मिलती है और उन्हें “कम जोखिम” वाला माना जाता है।
इसके विपरीत, विकासशील देश विदेशी मुद्राओं में कर्ज लेते हैं, उन्हें विनिमय दरों में भारी उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है और संकट के समय उनकी क्रेडिट रेटिंग घटा दी जाती है, जिससे उन्हें पूंजी जुटाने की लागत सबसे ज्यादा समय पर और बढ़ जाती है। अगर दुनिया सच में जलवायु कार्रवाई को गंभीरता से लेना चाहती है, तो उसे सबसे पहले अपनी टूटी-फूटी और बिखरी हुई वित्तीय व्यवस्था को ठीक करना होगा। खासकर कर्ज निपटाने की प्रक्रिया को न्यायपूर्ण, तेज और ठोस बनाना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (यूएनसीटैड) के एक विशेषज्ञ का कहना है कि फिलहाल जो तरीका अपनाया जा रहा है, वह पूरी तरह से ऋणदाताओं के नियंत्रण में है और जब कोई देश संकट में होता है तब यह तरीका उसकी नीति बनाने की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित करता है।
हाल के वर्षों में कुछ नीति विकल्प उभरे हैं, जो बड़ी व्यवस्था का कुछ-कुछ हल सुझाते हैं। इनमें एक है जी20 कॉमन फ्रेमवर्क, जो जी20 और पेरिस क्लब (पश्चिमी देशों के ऋणदाताओं का समूह) द्वारा समर्थित एक वैश्विक पहल है, जो सरकारों के कर्ज पुनर्गठन में मदद करती है। इसके अलावा कुछ विशेष रूप से जलवायु से संबंधित प्रस्ताव भी सामने आए हैं। इन्हीं में से एक उपाय है जलवायु के लिए कर्ज समझौते, दरअसल यह पहले के प्रकृति के बदले कर्ज मॉडलों का रूपांतर हैं। इनमें ऋणदाता देश किसी विकासशील देश के कर्ज का एक हिस्सा माफ कर देते हैं, बशर्ते वह देश उस बची हुई राशि को जलवायु लचीलापन या संरक्षण से जुड़े कार्यों में लगाए।
सेशेल्स, बेलीज, काबो वर्दे और बारबाडोस जैसे देशों में ऐसे सौदों का प्रयोग हुआ है और कुछ अच्छे नतीजे भी दिखे हैं। लेकिन अब तक ये उपाय छोटे पैमाने पर, धीमे और असंगठित तरीके से हुए हैं। ये किसी संप्रभु कर्ज राहत तंत्र का अभिन्न हिस्सा नहीं बन पाए हैं। इनकी आलोचना भी हुई है क्योंकि दुनिया के सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे 37 देश मिलकर भी वैश्विक उत्सर्जन का केवल 0.5 प्रतिशत हिस्सा ही करते हैं। इसके अलावा इन स्वैप्स के जरिए अब तक सिर्फ 3.7 अरब डॉलर का कर्ज ही माफ हुआ है, जो गरीब देशों के लिए कोई खास वित्तीय राहत नहीं बन सका। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक “सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट” के मुताबिक, इससे ज्यादा असरकारी उपाय कर्ज पर निर्भरता को कम करना, कर्ज प्रबंधन और जवाबदेही को बेहतर बनाना और कर्ज की संरचना और संचालन में सुधार करना हो सकता है। एक और नई पहल है “कर्ज स्थगन प्रावधान” यानी ऐसे अनुबंध प्रावधान जिनके तहत सरकारें जलवायु आपदा की स्थिति में कर्ज भुगतान को अस्थायी रूप से रोक सकती हैं। यह अस्थायी तरलता मुहैया कराता है, जब देश आपदा की मार झेल रहा हो।
बारबाडोस, ग्रेनेडा और बहामास जैसे देशों में इस मॉडल को अपनाया गया है। हालांकि, नागरिक समाज ने मौजूदा रूप में इनकी आलोचना की है, क्योंकि इनमें ब्याज तो लगातार जुड़ता रहता है, जबकि भुगतान रुका रहता है, इसलिए कुल कर्ज पर कोई असली राहत नहीं मिलती। इसके अलावा, ये प्रावधान सभी ऋणदाताओं के पास नहीं हैं और ये अनिवार्य भी नहीं हैं। इसलिए एक ऋणदाता से बचाए गए संसाधन को दूसरे को चुकाने में लगा देना आम बात है।
केन्या, कोलंबिया, फ्रांस और जर्मनी द्वारा संयुक्त तौर पर गठित “द एक्सपर्ट रिव्यू ऑन डेट, नेचर एंड क्लाइमेट” ने ऐसे सुझाव दिए हैं जो जलवायु-कर्ज के इस अंतर्संबंध की जड़ पर चोट करते हैं। उन्होंने विश्व बैंक और आईएमएफ द्वारा बनाए गए “कर्ज स्थिरता ढांचे” में सुधार की मांग की है, जो विकासशील देशों की ऋण स्थिति का मूल्यांकन करता है और यह तय करता है कि कोई देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कर्ज लेने योग्य है या नहीं। उनकी सलाह है कि इस मूल्यांकन में जलवायु जोखिम, प्रकृति से जुड़े जोखिम और विभिन्न जलवायु परिदृश्यों को शामिल किया जाए ताकि विश्लेषण ज्यादा मजबूत और जलवायु-संवेदनशील हो सके। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्ज माफी को भी बातचीत की मेज पर लाना होगा। “द जुबिली रिपोर्ट” यह जोर देती है कि ऋण का नकारात्मक शुद्ध प्रवाह रोकना जरूरी है। यानी ऐसी स्थिति जहां कोई देश जितना कर्ज चुकाता है, उससे बहुत कम सहायता या निवेश प्राप्त करता है। जब हर एक डॉलर की सहायता को दो डॉलर के कर्ज भुगतान से निष्प्रभावी कर दिया जाता है तब न तो मदद पर्याप्त होती है और न ही जलवायु वित्त।